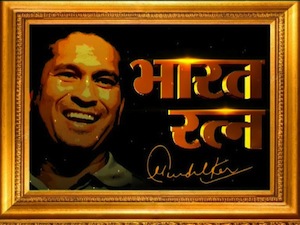हमारी संस्कृति में स्त्री को पुरुष की अर्धांगिनी कहा जाता है।अगर आँकड़ों की बात करें यह तो हमारे देश की आधी आबादी का प्रतिनिधित्व करती हैं।महिलाओं की स्थिति में सुधार के लिए अनेक कानून और योजनाएं हमारे देश में बनाई गई हैं लेकिन विचारणीय प्रश्न यह है कि हमारे देश की महिलाओं की स्थिति में कितना मूलभूत सुधार हुआ है।
चाहे शहरों की बात करें चाहे गांव की सच्चाई यह है कि महिलाओं की स्थिति आज भी आशा के अनुरूप नहीं है। चाहे सामाजिक जीवन की बात हो, चाहे पारिवारिक परिस्थितियों की,चाहे उनके शारीरिक स्वास्थ्य की बात हो या फिर व्यक्तित्व के विकास की,महिलाओं का संघर्ष तो माँ की कोख से ही शुरु हो जाता है।
जैसे ही पता चलता है कि आने वाला बच्चा लड़का नहीं लड़की है, या तो भ्रूण हत्या कर दी जाती है,और यदि चिकित्सीय अथवा कानूनी कारणों से यह संभव न हो तो, न तो शिशु के आगमन का इंतजार रहता है और न ही गर्भवती महिला के स्वास्थ्य की देखभाल की जाती है।जब एक स्त्री की कोख में एक अन्य स्त्री के जीवन का अंकुर फूटता है तो दो स्त्रियों के संघर्ष की शुरुआत होती है।
एक संघर्ष उस नवजीवन का जिसे इस धरती पर आने से पहले ही रौंदने की कोशिशें शुरू हो जाती हैं, और दूसरा संघर्ष उस माँ का जो उस जीवन के धरती पर आने का जरिया है।इस सामाजिक संघर्ष के अलावा वो संघर्ष जो उसका शरीर करता है, पोषण के आभाव में नौ महीने तक पल पल अपने खून अपनी आत्मा से अपने भीतर पलते जीवन को सींचते हुए।और इस संघर्ष के बीच उसकी मनोदशा को कौन समझ पाता है कि माँ बनने की खुशी, सृजन का आनंद, अपनी प्रतिछाया के निर्माण, उसके आने की खुशी, सब बौने हो जाते हैं ।
सामने अगर कुछ दिखाई देता है तो केवल विशालकाय एवं बहुत दूर तक चलने वाला संधर्ष , अपने स्वयं के ही आस्तित्व का।
और जब यह जीव कन्या के रूप में आस्तित्व में आता है तो भले ही हमारी संस्कृति में कन्याओं को पूजा जाता हो लेकिन अपने घर में कन्या का जन्म माथे पर चिंता की लकीरें खींचता है, होठों पर मुस्कुराहट की नहीं।तो जिस स्त्री को देवी लक्ष्मी अन्नपूर्णा जैसे नामों से नवाज़ा जाता है क्या उसे इन रूपों में समाज और परिवार में स्वीकारा भी जाता है?यदि हाँ तो क्यों उसे कोख में ही मार दिया जाता है?
क्यों उसे दहेज के लिए जलाया जाता है?
क्यों 2.5 से 3 साल तक की बच्चियों का बलात्कार किया जाता है?
क्यों कभी संस्कारों के नाम पर तो कभी रिवाजों के नाम पर उसकी इच्छाओं और उसकी स्वतंत्रता का गला घोंट दिया जाता है?कमी कहाँ है?हमारी संस्कृति तो हमें महिलाओं की इज्जत करना सिखाती है।हमारी पढ़ाई भी स्त्रियों का सम्मान करना सिखाती है।हमारे देश के कानून भी नारी के हक में हैं ।तो दोष कहाँ है?
आखिर क्यों जिस सभ्यता के संस्कारों में,सरकार और समाज सभी में,एक आदर्शवादी विचारधारा का संचार है,वह सभ्यता,इस विचारधारा को, इन संस्कारों को अपने आचरण और व्यवहार में बदल नहीं पा रही?
सम्पूर्ण विश्व में 8 मार्च को मनाया जाने वाला महिला दिवस एवं महिला सप्ताह केवल ‘कुछ’ महिलाओं के सम्मान और कुछ कार्यक्रमों के आयोजन के साथ हर साल मनाया जाता है।लेकिन इस प्रकार के आयोजनों का खोखलापन तब तक दूर नहीं होगा जब तक इस देश की उस आखिरी महिला के ‘सम्मान ‘ की तो छोड़िये, कम से कम उसके ‘स्वाभिमान’ की रक्षा के लिए उसे किसी कानून, सरकार, समाज या पुरुष की आवश्यकता नहीं रहेगी।वह ‘स्वयं’ अपने स्वाभिमान, अपने सम्मान, अपने आस्तित्व, अपने सपने, अपनी स्वतंत्रता की रक्षा करने के योग्य हो जाएगी।अर्थात वह सही मायनों में ‘पूर्ण रूप से आत्मनिर्भर’ हो जाएगी।
आज हमारे समाज में यह अत्यंत दुर्भाग्य का विषय है कि कुछ महिलाओं ने स्वयं अपनी ‘आत्मनिर्भरता ‘ के अर्थ को केवल कुछ भी पहनने से लेकर देर रात तक कहीं भी कभी भी कैसे भी घूमने फिरने की आजादी तक सीमित कर दिया है।
काश कि हम सब यह समझ पांए कि खाने पीने पहनने या फिर न पहनने की आजादी तो एक जानवर के पास भी होती है।
लेकिन आत्मनिर्भरता इस आजादी के आगे होती है,वो है खुल कर सोच पाने की आजादी,वो सोच जो उसे , उसके परिवार और समाज को आगे ले जाए,अपने दम पर खुश होने की आजादी,वो खुशी जो उसके भीतर से निकलकर उसके परिवार से होते हुए समाज तक जाए,इस विचार की आजादी कि वह केवल एक देह नहीं उससे कहीं बढ़कर है,यह साबित करने की आजादी कि अपनी बुद्धि, अपने विचार , अपनी काबलियत अपनी क्षमताओं और अपनी भावनाओं के दम वह अपने परिवार की और इस समाज की एक मजबूत नींव है।जरूरत है एक ऐसे समाज के निर्माण की जिसमेंयह न कहा जाए कि
“न आना इस देस मेरी लाडो ”
(डॉ नीलम महेंद्र)