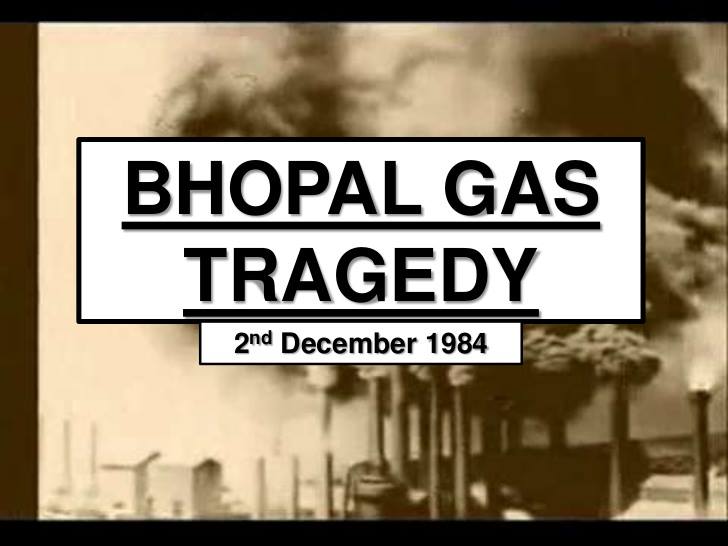मनोज कुमार
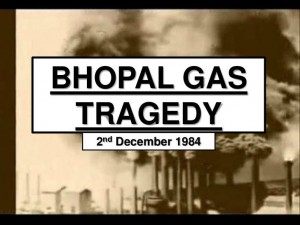
तीस बरस का समय कम नहीं होता है। भोपाल के बरक्स देखें तो यह कल की ही बात लगती है। 2-3 दिसम्बर की वह रात और रात की तरह गुजर जाती किन्तु ऐसा हो न सका। यह तारीख न केवल भोपाल के इतिहास में बल्कि दुनिया की भीषणतम त्रासदियों में शुमार हो गया है। यह कोई मामूली दुर्घटना नहीं थी बल्कि यह त्रासदी थी। एक ऐसी त्रासदी जिसका दुख, जिसकी पीड़ा और इससे उपजी अगिनत तकलीफें हर पल इस बात का स्मरण कराती रहेंगी कि साल 1984 की वह 2-3 दिसम्बर की आधी रात कितनी भयावह थी।
1984 से लेकर साल दर साल गुजरते गये। 1984 से 2014 तक की गिनती करें तो पूरे तीस बरस इस त्रासदी के पूरे हो चुके हैं। समय गुजर जाने के बाद पीड़ा और बढ़ती गयी। इसे एक किस्म का नासूर भी कह सकते हैं। नासूर इस मायने में कि इसका कोई मुकम्मल इलाज नहीं हो पाया या इस दिशा में कोई मुकम्मल कोशिशें नहीं हुई। इस पूरे तीस बरस में इस बात पर जोर दिया गया कि त्रासदी के लिये हमसे से कौन कसूरवार था? किसने यूनियन कार्बाइड के कर्ताधर्ता वारेन एंडरसन को भोपाल से दिल्ली और दिल्ली से उन्हें अपने देश भागने में मदद की? हम इस बात में उलझे रहे कि कसूरवार किसे ठहराया जाये लेकिन इस बात की हमने परवाह नहीं की जो लोग बेगुनाह थे, जिनकी जिंदगी में जहर घुली हवा ने तबाही मचा दी थी, जिनके सपने तो दूर, जिंदगी नरक बन गयी थी।
भोपाल गैस त्रासदी के नाम से कुख्यात हो चुके दुनिया की सबसे बड़ी औद्योगिक त्रासदी के इन तीस सालों को देखें और समझने का यत्न करें तो सरकारों और राजनीतिक दलों के लिये 2-3 दिसम्बर की तारीख रस्मी रह गयी है और मीडिया के लिये यह त्रासदी महज एक खबरनामा बन कर रह गयी है। 2-3 दिसम्बर की आधी रात का सच यह है कि अनगिनत बेगुनाहों को अकाल मौत के मुंह में समा जाना है तो 30 बरस का सच भी यही है। यह वही त्रासदी है जो राजनीतिक दलों के लिये खासा मायने रखती थी। हर बरस 3 दिसम्बर को सर्वधर्म सभा का आयोजन हुआ करता था। संवेदनाओं की गंगा बह निकलती थी। न्याय और हक दिलाने की बातें होती थी। इन तीस बरसों के हर चुनाव में गैस पीडि़त एक मुद्दा हुआ करते थे। जैसे जैसे साल गुजरता गया, गैस पीडि़त हाशिये पर जाते गये। चुनावी एजेंडे में अब गैस पीडि़त और गैस त्रासदी, त्रासदी न होकर महज एक दुर्घटना जैसी रह गयी थी।
अब रस्मी संवेदनायें होती हैं और अगले ही दिन जिंदगी पटरी पर आ जाती है। तीन दिसम्बर को जिस त्रासदी के दुख में भोपाली अवकाश मनाते हैं, उस दिन बाजार में रौनक कम नहीं होती है। सिनेमा घरों में न तो कोई शो बंद होता है और ना ही कोई आयोजन। दुख और पीड़ा उस परिवार की न तो पहले कम थी और न शायद जिंदगी के आखिरी सांस तक कम होगी क्योंकि जिन्होंने अपनों को खोया है, वे ही अपनों की दर्द समझ सकते हैं। ऐसे लोगों की तादात आज भी कम नहीं है जो जिंदा लाश बनकर अपनी मौत का इंतजार कर रहे हैं। यह मंजर बेहद डरावना और भयावह है। यह एक ऐसा सच है जो उस तारीख की आधी रात का था तो आज सुबह के उजाले में अपने सवालों के जवाब पाने के लिये खड़ा है।
कहने वाले तो कह सकते हैं कि आखिरी कब तक इस त्रासदी पर आंसू बहायेेंगे? यह कड़ुवी बयानबाजी से परहेज करने वाले कल भी थे और आज भी रहेंगे। याद करना होगा उस समय के हमारे संस्कृति सचिव महोदय आइएएस अधिकारी अशोक वाजपेयी को। वाजपेयी को याद करना इसलिये भी जरूरी है कि जिस तरह त्रासदी का यह दर्द जीवन में कभी नहीं भूलेगा, उसी तरह नश्तर की तरह चुभते उनके वह शब्द भी हवा में कभी विस्मृत नहीं हो पायेंगेे जब उन्होंने कहा था कि-‘मरने वालों के साथ मरा नहीं जाता है’। वाजपेयी एक संवेदनशील संस्कृति के संवाहक के रूप में हमारे साथ हैं लेकिन तब एक निष्ठुर प्रशासक के रूप में उन्होंने यह बयान देकर कराहते भोपाल में विश्व कविता समारोह का आयोजन सम्पन्न करा लिया था।
वाजपेयी जब यह बात कह रहे थे, तब इस बात का अंदाज समाज को नहीं रहा होगा कि आने वाले समय में विश्व की यह भीषणतम त्रासदी महज एक खबरनामा बन कर रह जायेगी। इस खबरनामा की शुरूआत अशोक वाजेपयी ने की थी और आज हम इस खबरनामा को महसूस कर रहे हैं।इन तीस सालों में अनेक किताबें बाजार में आ गयीं। लेखकों, रचनाकारों ने अपनी-अपनी रचना-धर्मिता का धर्म पूरा किया। अपने अपने स्तर पर त्रासदी को जांचने का प्रयास किया। किसी लेखक के केन्द्र में संवेदना थी तो कोई इसके दुष्परिणामों को जांच रहा था। कोई लेखक, लेखकीय सीमा से परे जाकर एक जासूस की तरह त्रासदी के लिये दोषियों को तलाश कर रहा था। गैस त्रासदी पर कुछेक छोटी प्रभावी फिल्में भी बनी और एक फीचर फिल्म भी परदे पर आ गयी। रचनाधर्मिता का यह पक्ष उजला-उजला सा है लेकिन सवाल है कि इस रचनाकर्म से किसकी नींद खुली और कौन पीडि़तों के पक्ष में खड़ा हुआ? यह सवाल भी जवाब की प्रतीक्षा में खड़ा ही रह जायेगा।
एक त्रासदी का खबरनामा से ज्यादा कुछ दिखायी नहीं देता और न ही महसूस किया जा सकता है। इस बात को और भी संजीदा ढंग से जांचना है तो यूनियन कार्बाइड के मुखिया वॉरेन एंडरसन की मौत की खबर एक सूचना की तरह प्रस्तुत की गयी। क्या एंडरसन की मौत से इस पूरे प्रकरण पर कोई गंभीर प्रभाव नहीं पड़ेगा? क्या इस बात पर मीडिया के मंच पर विमर्श नहीं होना चाहिये था? क्या एंडरसन की मौत एक आम आदमी की मौत थी? ऐसे अनेक सवाल हैं जो इस बात को स्थापित करते हैं कि विश्व की भीषणतम त्रासदी महज एक खबरनामा ही बन कर रह गयी है और यही सच है।भोपाल गैस त्रासदी के कई पहलु हैं जो समाज को आज भी झकझोर रहे हैं। इससे जुड़ा आर्थिक पक्ष तो है ही, सामाजिक जिम्मेदारी का पक्ष भी है जिसे अनदेखा नहीं किया जा सकता है। इस सिलसिले में अपना निजी अनुभव शेयर करना सामयिक लगता है।

इस त्रासदी की तीसरी बरसी थी। एक अखबारनवीस होने के नाते ह्यूमन स्टोरी की तलाश में जेपी नगर गया था। यहां मुलाकात होती है लगभग 11-12 वर्ष की उम्र के सुनील राजपूत से। सुनील की एक छोटी बहन और एक छोटे भाई को छोडक़र पूरा परिवार इस त्रासदी में अकाल मारा गया था। राहत के नाम पर मिले अकूत पैसों ने सुनील को बेपरवाह बना दिया था। हालांकि बाद के सालों में उसमें सुधार दिखा और इन पैसों से अपने छोटे भाई और बहन की जिम्मेदारी पूरी की किन्तु स्वयं मानसिक रूप से बीमार हो चुका था। सुनील की मृत्यु के कुछ समय पहले मेरी मुलाकात संभावना ट्रस्ट में हुयी थी जहां सुनील रहता था और उसका इलाज चल रहा था। सुनील एक उदाहरण मात्र है। ऐसे अनेक परिवार होंगे जो खबरों से दूर अपना दर्द अपने साथ समेटे जी रहे हैं।
त्रासदी के आरंभिक कुछ वर्ष छोड़ दिये जायें तो आमतौर पर 30 नवम्बर से 4 दिसम्बर तक अखबारों के पन्नों और टेलीविजन के परदे पर गैस त्रासदी से जुड़े मुद्दे पर विमर्श होता है।
सवाल यह है कि जिस त्रासदी को हम विश्व की भीषणतम औद्योगिक त्रासदी मान चुके हैं, जिस त्रासदी के शिकार लोगों को 30 बरस गुजर जाने के बाद भी न्याय और हक नहीं मिला है, जिस भोपाल की खुशियों को इस त्रासदी ने निगल लिया है, क्या इसे महज चंद दिनों के लिये हम खबरनामा बनने दें? शायद यह बात किसी को गंवारा नहीं होगी और न ही कोई इस तरह की पैरोकारी करेगा। यह त्रासदी महज एक औद्योगिक दुर्घटना नहीं बल्कि विकासशील समाज के समक्ष एक चुनौती है जिसे सामाजिक जवाबदारी के साथ ही पूरा किया जा सकेगा।
यह सवाल भी मौजूं है कि एक तरफ तो हम अभी भी भोपाल गैस त्रासदी से उबर नहीं पाये हैं और दूसरी तरफ उद्योगों का अम्बार लगाने के लिये बेताब हैं। औद्योगिकीकरण के लिये पूरा देश बेताब है और हर राज्य इन उद्योगों के लिये रेडकॉर्पेट बिछा रहा है। क्या हमने भोपाल गैस त्रासदी से कुछ सीखा है या इसे यूं ही हम भुला दे रहे हैं।
इन तीस साला सफर में एक बात का और अनुभव हुआ है। जिस वेदना के साथ हम इस त्रासदी का उल्लेख करते हैं, वह वेदना आज भी आम आदमी के भीतर है। वह उस त्रासदी की याद कर सिहर उठता है लेकिन वह लोग संवेदनहीन हो चुके हैं जो इस कालखंड में कमान सम्हाले हुये थे। फौरीतौर पर बयान देने के लिये अशोक वाजपेयी को इतिहास नहीं भुला पायेगा तो तत्कालीन भोपाल कलेक्टर मोतीसिंह की बातों को भुला पाना मुश्किल होगा जब गैस त्रासदी से जुड़े सवालों के जवाब में वे कहते हैं-छोड़ो इन बातों को, आओ, बनारस की बातें करें।
एक कहता है कि मरने वालों के साथ मरा नहीं जाता है, दूसरे को बनारस की याद आती है। सोच की यह दृष्टि हो तो गैस त्रासदी एक खबरनामा से अधिक रह भी नहीं जाती है। यह हमारे लिये दुर्भाग्य की बात है कि हम एक ऐसे समय में, एक ऐसे समाज में रह रहे हैं जहां परपीड़ा हमें सालती नहीं है। हम संवेदनहीन होते जा रहे हैं। अखबारों में छपने वाली खबरें हमें झकझोरती नहीं हैं और ऐसे में भोपाल त्रासदी, खबरनामा ही बन कर रह जाये तो शिकायत किससे और कैसी?
(लेखक भोपाल से प्रकाशित शोध पत्रिका समागम के संपादक है.)