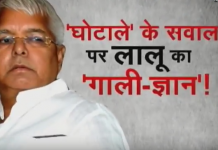खास व्यंजन को खास जाति से क्यों जोड़ा जाये ?
 लीना/ एक बुजुर्ग रचनाकार ने हिन्दी पत्रिका ‘शुक्रवार’ के 11 जुलाई 2013 के अंक में अपने नियमित खान-पान स्तंभ में गर्व के साथ अफसोस जताया है कि एक खास जाति के खाने को उस खास जाति वाले ही तजने लगे हैं। बड़े ही गर्व से उन्होंने खास जाति के खान-पान की परंपरा के विकास को बताया है। यही नहीं, खान-पान की परंपरा बताने से पहले वे इस कुल में जन्म लेने वाले लोग विद्वान, साहित्यकार, प्रबंधक आदि यानी कि बु्द्धिजीवी होते हैं, यह तारीफ करना भी नहीं भूले हैं। उन्हें तरक्की पसंद, यथार्थवादी सोच वाला भी बताया है।
लीना/ एक बुजुर्ग रचनाकार ने हिन्दी पत्रिका ‘शुक्रवार’ के 11 जुलाई 2013 के अंक में अपने नियमित खान-पान स्तंभ में गर्व के साथ अफसोस जताया है कि एक खास जाति के खाने को उस खास जाति वाले ही तजने लगे हैं। बड़े ही गर्व से उन्होंने खास जाति के खान-पान की परंपरा के विकास को बताया है। यही नहीं, खान-पान की परंपरा बताने से पहले वे इस कुल में जन्म लेने वाले लोग विद्वान, साहित्यकार, प्रबंधक आदि यानी कि बु्द्धिजीवी होते हैं, यह तारीफ करना भी नहीं भूले हैं। उन्हें तरक्की पसंद, यथार्थवादी सोच वाला भी बताया है।
तो क्या वेद पुराणों का हवाला देकर समाज में सदियों से मौजूद जातिभेद के आधार पर खास कार्य क्षेत्र की वकालत करने वाले सवर्ण अब खास व्यंजन और पकवानों पर भी अपना अधिकार जताने लगे हैं। लोक मान्यता का हवाला देकर नई नई मान्यताएं भी गढ़ने लगे हैं।
बुजुर्ग रचनाकार ने कई व्यंजनों के नाम गिनाए हैं, जिसमें इस खास जाति के परिवार के पकाने के अपने विशेष नुस्खे हैं और जिनकी लज्जत का जबाव नहीं। कोई उनसे पूछे या वो बताये कि कोफ्ते, कलेजी पुलाव किस जाति के लोग नहीं पकाते-खाते रहे हैं या कि मुर्गी-बटेर कौन सा जात नहीं खाता रहा है?
लेकिन अगर हम ऐतिहासिक संदर्भ भी लें तो नरगिसी कोफ्ता अवधी और मलाई कोफ्ता मुगलई व्यंजन है। इसी तरह सालन या रसदार सब्जियां भी अलग अलग प्रदेशों के अनुसार ही बनाई जाती हैं। मसलन खट्टी अरबी की सालन दक्षिण भारत में मशहूर है। और वर्तमान संदर्भ की भी बात करें तो भी जातिगत आधार पर खास व्यंजन बनाने का जिक्र शायद ही कहीं दिखता है।
जिस गुलगुले का उन्होंने जिक्र किया है, बचपन में हमने सभी प्रकार के घरों में खाया है, चाहे वे किसी जाति वाले हों। हां ये अलग बात हे कि कई अन्य पारंपरिक पकवानों की तरह गुलगुले पकाने की परंपरा भी घरों में अब खतम होती जा रही है। उसी तरह अरबी के पत्तों वाली सब्जी भी पकायी-खाई है और चाव से बेसन का बना ‘धोखा’ भी खाया है।
इसमें कोई शक नहीं कि अलग-अलग लोगों के हाथों से बने व्यंजन का स्वाद अलग होता है। लेकिन खाने पीने की चीजें, बनाने का तरीका और पारंपरिक व्यंजन पर जाति विशेष का नहीं, जगह विशेष का फर्क पड़ता है। भले ही आर्थिक हैसियत से इनकी लजीजता में फर्क आये, लेकिन किसी भी राज्य या क्षेत्र के हिसाब से ही खास व्यंजन पकाये जाने की परंपरा ही देखी जाती है। लिट्टी-चोखा बिहार की पहचान है ना कि किसी जाति की। ढोकला को गुजराती व्यंजन कहा जाता है, तो डोसा दक्षिण भारतीय माना जाता है। वैसे ही, जैसे कि मक्के की रोटी और सरसों का साग का नाम आते ही पंजाब याद आता है ना कि किसी जाति विशेष का।
भले ही ये बुजुर्ग रचनाकार देश विदेश के व्यंजनों पर लिखने की काबिलियत रखतें हों, लेकिन खास व्यंजनों पर खास जाति की मुहर लगाने जैसी असामाजिक सिद्धांत गढ़ने का उन्हें कोई हक नहीं है। उस पर तुर्रा यह है कि उन्हें किसी परिवार में धुस्का और आलूदम खा के ही ‘आशा की किरण’ भी नजर आने लगती है।