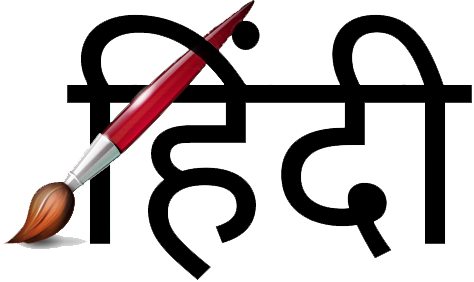अब लडाई अंग्रेजी को हटाने की नहीं हिंदी को बचाने की है
संजय द्विवेदी
सरकारों के भरोसे हिंदी का विकास और विस्तार सोचने वालों को अब मान लेना चाहिए कि राजनीति और सत्ता से हिंदी का भला नहीं हो सकता। हिंदी एक ऐसी सूली पर चढ़ा दी गयी है, जहां उसे रहना तो अंग्रेजी की अनुगामी ही है। आत्मदैन्य से घिरा हिंदी समाज खुद ही भाषा की दुर्गति के लिए जिम्मेदार है। हिंदी को लेकर न सिर्फ हमारा भरोसा टूटा है बल्कि आत्मविश्वास भी खत्म हो चुका है। यह आत्मविश्वास कई स्तरों पर खंडित हुआ है। हमें और हमारी आने वाली पीढियों को यह बता दिया गया है कि अंग्रेजी के बिना उनका कोई भविष्य नहीं है। हमारी सबसे बड़ी अदालत भी इस देश के जन की भाषा को न तो समझती है, न ही बोलती है। ऐसे में सिर्फ मनोरंजन और वोट मांगने की भाषा भर रह गयी हिंदी से आप क्या उम्मीद कर सकते हैं।
सरकारों का संकट यह है कि वे चीन, जापान, रूस जैसे तमाम देशों के भाषा प्रेम और विकास से अवगत हैं किंतु वे नई पीढ़ी को ऐसे आत्मदैन्य से भर चुके हैं कि हिंदी और भारतीय भाषाओं को लेकर उनका आत्मविश्वास और गौरव दोनों चकनाचूर हो चुका है। आप कुछ भी कहें हिंदी की दीनता जारी रहने वाली है और यह विलाप का विषय नहीं है। महात्मा गांधी के राष्ट्रभाषा प्रेम के बाद भी हमने जैसी भाषा नीति बनाई वह सामने है। वे गलतियां आज भी जारी हैं और इस सिलसिले की रुकने की उम्मीदें कम ही हैं। संसद से लेकर अदालत तक, इंटरव्यू से लेकर नौकरी तक, सब अंग्रेजी से होगा तो हिंदी प्रतिष्ठित कैसे होगी? आजादी के सत्तर साल बाद अंग्रेजी को हटाना तो दूर हम हिंदी को उसकी जगह भी नहीं दिलवा पाए हैं। समूचा राजनीतिक, प्रशासनिक, न्यायिक तंत्र अंग्रेजी में ही सोचता, बोलता और व्यवहार करता है। ऐसे तंत्र में हमारे भाषाई समाज के प्रति संवेदना कैसे हो सकती है। उनकी नजर में हिंदी और अन्य भारतीय भाषाएं एक वर्नाक्यूलर भाषाएं हैं। ये राज काज की भाषा नहीं है। कितना आश्चर्य है कि जिन भाषाओं के सहारे हमने अपनी आजादी की जंग लड़ी, स्वराज और सुराज के सपने बुने, जो केवल हमारे सपनों एवं अपनों ही नहीं अपितु आकांक्षाओं से लेकर आर्तनाद की भाषाएं हैं, उन्हें हम भुलाकर अंग्रेजी के मोहपाश से मुक्त नहीं हो पा रहे हैं।
हिंदी दिवस मनाता समाज यह बता रहा है कि हम कहां हैं? यह बात बताती है कि दरअसल हिंदी के लिए बस यही एक ही दिन बचा है, बाकी 364 दिन अंग्रेजी के ही हैं। यह ढोंग और पाखंड हमारी खूबी है कि हम जिसे जी नहीं सकते, उसके उत्सव मनाते हैं। घरों से निष्काषित हो रही, शिक्षा से हकाली जा रही हिंदी अब दिनों, सप्ताहों और पखवाड़ों की चीज है। यह पाखंड पर्व निरंतर है और इससे हिंदी का कोई भला नहीं हो रहा है। राजनीति, जिससे उम्मीदें वह भी पराजित हो चुकी है।
समाजवादियों से लेकर राष्ट्रवादियों तक ने भाषा के सवाल पर अपने मूल्यों से शीर्षासन कर लिया है। अब उम्मीद किससे की जाए? इस घने अंधेरे में महात्मा गांधी, डा. राममनोहर लोहिया, पुरूषोत्तमदास टंडन जैसे राजनेता और मार्गदर्शक हमारे बीच नहीं हैं। जो हैं भी वे सब के सब आत्मसमर्पणकारी मुद्रा में हैं। कभी लगता था कि कोई अहिंदी भाषी देश का प्रधानमंत्री बनेगा तो हिंदी के दिन बहुरेगें। लेकिन लगता है वह उम्मीद भी अब हवा हो चुकी है। राजनेताओं ने जिस तरह से अंग्रेजी के आतंक के सामने आत्मसमर्पण किया है, वह एक अद्भुत कथा है। वहीं हिंदी समाज भी लगभग इसी मुद्रा में है। इसलिए राजनीति और उसके सितारों से हिंदी को कोई उम्मीद नहीं पालनी चाहिए। नया दौर इस अंग्रेजी और अंग्रेजियत को पालने-पोसने वाला ही साबित हुआ है। हमारे समय के एक बड़े कवि सर्वेश्वर दयाल सक्सेना लिखते हैं- “दिल्ली हमका चाकर कीन्ह, दिल दिमाग भूसा भर दीन्ह।”
हिंदी में वोट मांगते और हिंदी के सहारे राजसत्ता पाने वाले ही, दिल्ली पहुंचकर सबसे पहले देश की भाषा को भूलते हैं और उन्हें प्रशासनिक तंत्र के वही तर्क रास आने लगते हैं, जिसकी पूर्व में उन्होंने सर्वाधिक आलोचना की हुई होती है। दिल्ली उन्हें अपने जैसा बना लेती है। अनेक हिंदी भक्त प्रधानमंत्री के पद तक पहुंचे पर हिंदी तो वहीं की वहीं है, अंग्रेजी का विस्तार और प्रभाव कई गुना बढ़ गया। लार्ड मैकाले जो नहीं कर पाए, वह हमारे भूमि पुत्रों ने कर दिया और गांव-गांव तक अंग्रेजी माध्यम के स्कूल खुल गए। अंग्रेजी सिखाना एक उद्योग में बदल गया। अंग्रेजी न जानने के कारण आत्मविश्वास खोकर इस देश की नौजवानी आत्महत्या तक करती रही, लेकिन सत्ता अपनी चाल में मस्त है।
ऐसे में भरोसा फिर उन्हीं नौजवानों का करना होगा जो एक नए भारत के निर्माण के लिए जुटी है। जो अपनी जड़ों की ओर लौटना चाहती है। जो जड़ों में मुक्ति खोज रही है। भरोसे और आत्मविश्वास से दमकते तमाम चेहरों का इंतजार भारत कर रहा है। ऐसे चेहरे जो भारत की बात भारत की भाषाओं में करेंगे। जो अंग्रेजी में दक्ष होंगे, किंतु अपनी भाषाओं को लेकर गर्व से भरे होंगे। उनमें हिंदी मीडियम टाइप (एचएमटी) या वर्नाकुलर पर्सन कहे जाने पर दीनता पैदा नहीं होगी बल्कि वे अपने काम से लोगों का, दुनिया का भरोसा जीतेंगे। हिंदी और भारतीय भाषाओं की विदाई के इस कठिन समय में देश ऐसे युवाओं का इंतजार कर है जो अपनी भारतीयता को उसकी भाषा, उसकी परंपरा, उसकी संस्कृति के साथ समग्रता में स्वीकार करेंगे। जिनके लिए परम्परा और संस्कृति एक बोझ नहीं बल्कि गौरव का कारण होगी।
एक युवा क्रांति देश में प्रतीक्षित है। यह नौजवानी आज कई क्षेत्रों में सक्रिय दिखती है। खासकर सूचना-प्रौद्योगिकी की दुनिया में। जिन्होंने इस भ्रम को तोड़ दिया कि आई टी की दुनिया में बिना अंग्रेजी के गुजारा नहीं है। ये लोग ही भरोसा जगा रहे हैं। ये भारत को भी जगा रहे हैं। एक गुजराती भाषी अपनी राष्ट्रभाषा में ही इस देश को संबोधित कर प्रधानमंत्री बना है। भरोसा जगाते ऐसे कई दृश्य हैं अमिताभ बच्चन हैं, प्रसून जोशी हैं, बाबा रामदेव, नरेंद्र कोहली हैं, लता मंगेश्कर हैं। जिनके श्रीमुख और कलम से मुखरित-व्यक्त होती हिंदी ही तो देश की ताकत है। आजादी के सात दशक के बाद हिंदी दिवस मनाने के बजाए हम हिंदी को उसका वास्तविक स्थान दिलाने, घरों और नई पीढ़ी तक हिंदी और भारतीय भाषाओं को पहुंचाने का काम करें तो ही अंग्रेजी के विस्तारवाद से लड़ सकेंगे। अब लड़ाई अंग्रेजी को हटाने की नहीं, हिंदी और भारतीय भाषाओं को बचाने की है, अपने घर से बेधर न हो जाने की है।
(लेखक माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय, भोपाल में जनसंचार विभाग के अध्यक्ष हैं।)