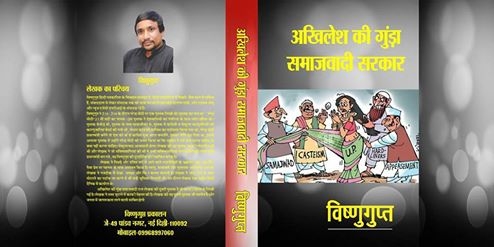हम प्रिंट के लिए अब क्यों नहीं लिखना चाहते ? मैं कोई बड़ा लेखक नहीं हूं और न ही मेरी कोई बड़ी हैसियत है. बस ये है कि लिखना मेरे लिए ऑक्सीजन जुटाने जैसा है. बिना लिखे रह नहीं सकता. ये मेरे पेशे की, मेरे मन की, खुद मेरी जरूरत है. बावजूद इसके प्रिंट मीडिया जिसमे सरोकारी साहित्यिक पत्रिकाओं से लेकर व्यावसायिक अखबार तक शामिल हैं, के लिए लिखने का बिल्कुल मन नहीं करता. मैंने बहुत पहले तय भी किया था कि अब धीरे-धीरे करके इनके लिए लिखना बिल्कुल बंद कर देना है. तहलका, जनसत्ता जैसे मंचों के लिए न लिखने की वजह यही रही.
ऐसा कहना या इस फैसले तक पहुंचना किसी भी तरह के बड़बोलेपन या अहंकार का हिस्सा नहीं है. ये मेरी अपनी कमजोरी है. ब्लॉगिंग के दौर से जो मेरी थोड़ी-बहुत पहचान बनी और लोग लिखने के मौके देने लगे तो मैं लिखने लग गया. एक समय में खूब लिखा और धीरे-धीरे ऐसे दवाब में आता चला गया कि मेरी नींद, मेरा आराम, मेरा शरीर सब दांव पर लगने लग गए. न्यूजरूम की उनकी परेशानी और डेडलाइन प्रेशर मेरे उपर आने लग गए. मैं देखते-देखते प्रिंट मीडिया फोबिया का शिकार हो गया. मैं दिनभर बाकी के काम करता लेकिन दिमाग में डेडलाइन घूमती रहती.
जो भी लिखने कहते, पहले उनमे आग्रह होता, दोस्ती-यारी का हवाला होता और जैसे-जैसे समय नजदीक आता, वो सख्त होते चले जाते. कुछ का अंदाज इस तरह होता कि जैसे मैंने उनसे कर्ज लिया हुआ हो. आप कह सकते हैं कि मैं ऐसा लिखकर प्रोफेशनलिज्म और उसकी शर्तों से भाग रहा हूं. लेकिन यदि समय पर लेख देना प्रोफेशनलिज्म है तो लेख छपने के बाद सौ रूपये तक भी न देना सामाजिक सरोकार और हिन्दी सेवा कैसे हो गई ? तथाकथित सरोकारी और साहित्यिक पत्रिकाओं के लिए एक लेख लिखने में मैं डेढ़ से दो महीने उससे बुरी तरह जूझता रहता. एक लेख पर चार-पांच हजार रूपये किताब, फोटोकॉपी और सामग्री जुटाने में खर्च हो जाते. ताबड़तोड़ फोन कॉल के बीच जब वो लेख छपकर सामने आता तो पत्रिका की कॉपी तक नहीं मिलती. कुछ की प्रति के साथ एक चिठ्ठी शामिल होती जिसमे लिखा होता कि हमने आपके पारिश्रमिक के तौर पर पत्रिका की एक साल की सदस्यता दे दी है. मैं उस पत्रिका का सदस्य बनना चाहता भी हूं नहीं, ये सब बिना जाने-समझे ही.
खैर, हिन्दी की समाज सेवा से हम धीरे-धीरे छूटने लगे. शुरू में नामचीन चेहरे का लिहाज करके लिखता रहा. बाद में वो लिहाज करना भी छोड़ दिया. हमने कई मोर्चे पर महसूस किया कि उन्होंने अपने लेखक के हक के लिए लड़ना छोड़ दिया. लिहाजा, अब लिखने की बात करते ही अब हाथ जोड़ लेता हूं. बस इसलिए कि मुझ पर इन सबका गहरा असर होता है. मैंने एक-एक लेख के पीछे कितनी रातें खराब की है. अपनी भूख, नींद, आराम सबकुछ. कई बार बीमार भी होते रहे.
इधर अखबार और पत्रिकाओं के लिए ज्यादातर दोस्ती और भावनात्मक स्तर पर जुड़ाव के कारण लिखता रहा जो कि अब तेजी से खत्म हो रहा है. अब सच पूछिए तो किसी से जुड़ाव महसूस ही नहीं होता क्योंकि इसका कोई मोल रहा ही नहीं है शायद. हम अब तक इस दोस्ती में, लिहाज में और अपने लोगों तक बात पहुंचाने की ललक में प्रिंट मीडिया के लिए लिखते रहे. लेकिन अब मेरे लिए ऐसा कर पाना बिल्कुल भी संभव नहीं है. ऑर्डर पर बताशे और गुलगुले बनाने का काम मुझसे नहीं हो पाता. वर्चुअल स्पेस पर लगातार लिखते रहने से अच्छा-बुरा जैसा भी है, अपना एक अंदाज पनपने लग गया है. मैं उस अंदाज में लिखकर खुश रहता हूं. नौकरी के लिए जितना शोधपरक,सार्थक लेखन करना था, हो लिया. चालीस से ज्यादा कॉलेजों के इंटरव्यू में उन फाइलों को ढोते-ढोते मेरी कलाइयों में अब दर्द रहने लगा है. हर दूसरे-तीसरे इंटरव्यू में यही लगता है कि काश भीतर को ऐसा शख्स हो जो कहे कि- अरे रहने दो फाइल-वाइल, मैंने तुम्हारा लिखा पढ़ा है.
आप इसे एक हताश-निराश व्यक्ति का वक्तव्य कह लें या फिर एक बड़बोले शख्स का गैरजरूरी बयान..लेकिन मुझे अब इतनी ही बात समझ आती है कि किसी अखबार या पत्रिका के लिए अमुक विषय पर लेख छापना या लिख देने के बाद नहीं छापने की मजबूरी है तो उस दवाब को मैं क्यों झेलूं. न्यूजरूम के दवाब को मैं अपने उपर क्यों हावी होने दूं ? ठीक उसी तरह किसी सरोकारी व्यक्ति को पत्रिका का संपादक बनकर हिन्दी सेवा करनी है जो कि मुझे नहीं करनी है तो मैं उसकी इस संतई में क्यों परेड करने लग जाउं.
मेरी अपनी समझ बिल्कुल साफ है. यदि मैं शौक और दिमागी जरूरत के लिए लिखता हूं तो मुझे पहले अपनी सेहत और पसंद का ख्याल रखना होगा. और यदि मैं पैसे के बजाय पाठकों तक अपनी बात पहुंचाने के लिए लिख रहा हूं तो फेसबुक, वर्चुअल स्पेस की दुनिया पर्याप्त है. लेकिन जो काम धंधे के लिए किया जा रहा हो, उसमे मैं आखिर संत बनकर क्यों शामिल हो जाउं. वहां के लिए लिख रहा हूं तो मुझे पैसे चाहिए, मुझे वो सबकुछ चाहिए जिसकी उम्मीद मेरा प्लम्बर, इलेक्ट्रिशियन और सिक्यूरिटी गार्ड करता है. लिखनेवाले की दीहाडी मारकर यदि आप उसे हिन्दी सेवक घोषित करने में लगे हैं तो माफ कीजिएगा, मैं उस बिरादरी से बाहर का आदमी हूं.
हिन्दी पखवाड़ा सीरिज- 1