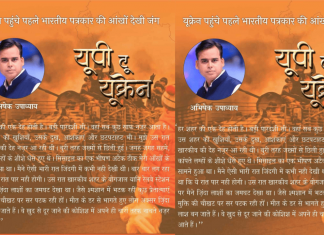प्रियदर्शन
समकालीन हिंदी मीडिया की चुनौतियों पर इतनी बार और इतनी तरह से चर्चा हो चुकी है कि इस पर फिर से बात करना भी एक चुनौती लगता है। सिर्फ इसलिए नहीं कि इस मुद्दे पर नया कुछ कहने को बाक़ी नहीं है, बल्कि इसलिए भी कि जिन चुनौतियों की हम पहले चर्चा करते रहे हैं, उनका सामना करने की इच्छाशक्ति तो दूर, इच्छा भी मीडिया नहीं दिखाता। आम तौर पर टीवी चैनलों की चर्चा होते ही एक आत्मनिरीक्षण का दौर सा चल पड़ता है। ढेर सारे लोग यह बताने वाले निकल पड़ते हैं कि मीडिया पर पड़ने वाले दबावों से कैसे निबटने की ज़रूरत है और किस तरह मीडिया का सतहीपन बढ रहा है। दिलचस्प यह है कि यह बात- जाहिर है, बहुत प्रामाणिकता के साथ- वे लोग बताते हैं जो मीडिया के इस खेल में बहुत भीतर तक उतरे हुए हैं, उसके बनाए नायक हैं। लेकिन इतनी चुनौती-चर्चा, इतने पश्चातापी आत्मनिरीक्षण के बावजूद यह नज़र नहीं आता कि कोई बदलने को तैयार है। सपाटपन और सतहीपन के समंदर में कभी-कभार विचार और कल्पनाशीलता के एकाध संवेदनशील टापू दिख जाएं तो मीडिया उन्हीं की तरफ इशारा करता हुआ उसे समग्रता के प्रमाण की तरह पेश करने में जुट जाता है।
तो मेरी समझ में समकालीन मीडिया की सबसे बड़ी चुनौती तो यही है कि वह अपनी चुनौतियों से लड़ने की जैसे ताकत खो बैठा है। मीडिया के मालिक या तो ख़ुद संपादक हैं या फिर ऐसे संपादक रख रहे हैं जो सिर्फ उनकी सुने। इन नए संपादकों की योग्यता का पैमाना उनका ज्ञान, उनका कौशल नहीं, उनके संपर्क हैं, उनकी जान-पहचान है, उनकी राजनीतिक ताकत है। आज मीडिया घरानों के भीतर का कोई बडा और संवेदनशील पत्रकार अपने संपादक होने की कल्पना नहीं कर सकता, बशर्ते उसकी सिफ़ारिश किसी बड़े और नामी-गिरामी दूसरे संपादक ने नहीं की हो। जो बाकी पत्रकार हैं, वे नौकरी बजा रहे हैं और उदारीकरण के इस बदले हुए दौर में, छंटनी और बंदी की तलवारों से बचते हुए, ख़ुद को ख़ुशक़िस्मत मानते हुए, बस अख़बार बना रहे हैं, टीवी के बुलेटिन तैयार कर रहे हैं। टीवी चैनलों पर बड़ी हड़बड़ाहट के साथ आने-जाने और बदलने वाली ब्रेकिंग न्यूज़ की पट्टियों के पीछे जिस तरह की ऊब, एकरसता और यांत्रिकता हावी है, उसे वही लोग महसूस करते हैं जो वहां काम करते हैं।
सवाल है, ऐसा क्यों हो रहा है। मीडिया का चरित्र अचानक इस तरह क्यों बदल गया है? इस सवाल का जवाब मीडिया के भीतर नहीं, मीडिया से बाहर उस समाज के भीतर खोजना होगा जिसके बीच मीडिया बनता है। बीती सदी के आख़िरी दशक में आए और इक्कीसवीं सदी में हर तरफ़ छा और छितरा गए आर्थिक उदारीकरण की बहुत सारी सौगातें मॉल, मल्टीप्लेक्स, विदेशी ब्रांड्स और नए शोरूम्स की शक्ल में हमारे सामने हैं और इस उदारीकरण ने इनके उपभोग के लिए हर महीने लाखों कमाने वाला बीस-पच्चीस करोड़ का एक उच्च मध्यवर्गीय भारत भी पैदा कर दिया है। यह नया भारत- जो यह कल्पना करता है कि आने वाले दशकों में वह एक विश्वशक्ति होगा- इस उदारीकरण का इंजन भी बना हुआ है और इसकी अलग-अलग बोगियों में भी बैठा हुआ है। हमारे अखबार, हमारे टीवी चैनल, हमारे पत्रकार और हमारे संपादक इन दिनों इसी वर्ग से आ रहे हैं और इसी वर्ग के लिए समर्पित हैं। जो अभी तक इसके दायरे से बाहर हैं, उनके भीतर भी यही कामना है कि वे इसमें किसी न किसी तरह शामिल हो जाएं। इस नए भारत को सूचना प्रौद्योगिकी के इस विराट दौर में सबकुछ अपनी उंगलियों पर, अपने मोबाइल पर, अपने ऐप्स की शक्ल में चाहिए। उसे 24 घंटे मनोरंजन चाहिए, खाने-पीने-घूमने का बेरोकटोक इंतज़ाम चाहिए, चिकनी-फिसलती सड़कें चाहिए, बड़ी चमचमाती गाड़ियां चाहिए और ऐसी चटपटी ख़बरें चाहिए जिन्हें पढ़ते-देखते हुए वह या तो अपने भारत पर गर्व कर सके या फिर दूसरे भारत को हिकारत से देख सके- यह सोचते हुए कि अच्छा हुआ कि उसका पीछा इस गंदी-गंधाती-बजबजाती दुनिया से छूटा।
इस नए भारत में 24 घंटे ख़बरें बेचने निकला मीडिया ख़बरों का चयन भी अपनी प्राथमिकता के हिसाब से करता है और उनकी प्रस्तुति में भी वह हल्का-फुल्कापन बनाए रखता है जो उसके पहले से तनावग्रस्त तबके का तनाव न बढ़ाए। उसके सरोकारों के दायरे में दिल्ली या दिल्ली जैसे महानगरीय चरित्र वाले दूसरे शहरों के वाशिंदे आते हैं, उनके साथ हुई नाइंसाफ़ी की ख़बर उसे चुभती है, उसके हाथ से छीन लिए जाने वाले मौके उसे सालते हैं, लेकिन उसके दायरे से बाहर जो बहुत विशाल भारत है, उसकी चीखें वह नहीं सुनता, उसकी रुलाइयां वह नहीं देखता, उसकी ख़बर वह नहीं लेता। दिल्ली के एक मॉल से फिल्म देखकर निकल रही एक लड़की के साथ हुआ सामूहिक बलात्कार इसीलिए राष्ट्रीय शर्म और उत्तेजना का विषय बन जाता है, जबकि इसी दिल्ली की झुग्गियों में छोटी बच्चियों के साथ जो कुछ होता है, वह आई-गई ख़बर की तरह ले लिया जाता है। जब मणिपुर और छत्तीसगढ़ में औरतें सताई जाती हैं तो वह उसकी ख़बर टाल कर आगे बढ़ जाता है।
ख़बरों का चयन ही नहीं, उनका परिप्रेक्ष्य भी इसी वर्गीय चेतना से तय होता है। अब पानी बरसने की ख़बर मीडिया के लिए दिल्ली में जाम लगने की ख़बर होती है, मौसम की फसल के लिए फायदे या नुकसान की नहीं। फेसबुक और ट्विटर पर लगी पाबंदी अभिव्यक्ति की आज़ादी का हनन बन जाती है (जो बेशक वह है), लेकिन प्रतिरोध के दूसरे आंदोलनों की पीठ पर पड़ती लाठी और सीने पर पड़ती गोलियां लोकतंत्र पर ख़तरे की वह गूंज पैदा नहीं करतीं। राजनीतिक भ्रष्टाचार बड़ी सुर्खी बनता है, जबकि दफ़्तरों, कचहरियों और निजी कंपनियों की ठेका लूट का भ्रष्टाचार किनारे कर दिया जाता है। दिल्ली के जंतर-मंत पर अण्णा हज़ारे का आंदोलन बड़ा हो जाता है, मणिपुर में शर्मिला इरोम के अनशन पर नज़र नहीं पड़ती।
लेकिन जब दुनिया ऐसी है और मीडिया ऐसा है तो उसकी चुनौती कैसी और उसपर सवाल क्यों? अगर वह निजी पूंजी का मुनाफादेह उद्यम है और ऐसी ही ख़बरों से उसका काम चल रहा है तो किसी और को उसपर एतराज़ करने का हक़ क्या है?
लेकिन यह हक़ है। क्योंकि मीडिया का दावा तो सबकी नुमाइंदगी का है। इसी दावे पर वह खुद को अखिल भारतीय बताता है, जनपक्षीय बताता है, सबकी ख़बर लेने-देने वाला, सबसे तेज़, सबसे आगे बनता है, लोगों को वादा करता है कि वह सूचनाओं में उनको सबसे आगे रखेगा। हालांकि यहां से देखें तो यह सिर्फ दावा नहीं, एक दुविधा भी है। मीडिया का वर्तमान जो भी हो, इस देश में मीडिया की विरासत बहुत बड़ी रही है। भारतीय पत्रकारिता अंग्रेजों के साथ लोहा लेती हुई जेलखानों में पैदा हुई और पली-बढ़ी। देश और समाज को समझने और सिरजने का जज़्बा उसके भीतर इसी गुणसूत्र से आया है। इसी जीन ने मीडिया के भीतर यह ताकत पैदा की कि वह भारतीय लोकतंत्र का चौथा खंभा बने और जब बाकी खंभे भरोसा खो रहे हों तो भी वह अपना भरोसा बनाए रखे। अपनी सारी मुश्किलों, नाकामियों, अपने सारे बेतुकेपन के बावजूद भारतीय लोकतंत्र का जो एक आज़ाद, खुला मिज़ाज है, वह बहुत कुछ इस मीडिया की वजह से भी है। आज भी इस मीडिया में प्रतिरोध की बहुत सारी आवाज़ें हैं जो लगातार इस बात की तरफ ध्यान खींच रही हैं कि नए दौर की यह बाज़ार-व्यवस्था अपने चरित्र में सामुदायिकता विरोधी है, समता विरोधी है और अंततः लोकतंत्र विरोधी है। यह दुनिया को लूटने निकली है और इस लूट के विरुद्ध उठने वाली, इसका पर्दाफ़ाश करने वाली हर आवाज़ को कुचलना, अविश्वसनीय बनाना, और अपनी ज़रूरतों के हिसाब से ढालना भी उसका लक्ष्य है।
दरअसल इस मोड़ पर आकर मीडिया की सबसे बड़ी चुनौती को पहचान सकते हैं। लेख के शुरू में जो सवाल था कि हम अपनी चुनौतियों को पहचानते हुए भी उनसे मुठभेड क्यों नहीं कर पा रहे, उसका एक जवाब यहां छुपा है। नए ज़माने की पूंजी और सत्ताएं आवाज़ों को दबाने के सौ तरीके जानती हैं। उन्हें मालूम है कि लोगों को जेल में डालना, पत्रकारों पर सीधी रोक लगाना, मीडिया की बांहें उमेठना उन्हें ज़्यादा भरोसा दिलाना है, उनकी बात को सही साबित करना है। उनको रोकने का ज़्यादा सही तरीक़ा यह है कि उन्हें इस व्यवस्था का पुर्जा बना लिया जाए। थोड़ी सी आज़ादी के भरम और बहुत अच्छी सैलरी की हक़ीक़त के बीच फंसा पत्रकार धीरे-धीरे अपना वर्ग चरित्र भी भूलने लगता है और नए माहौल में ढलने लगता है। अचानक नई कारों पर लगने वाला टैक्स, घरों के क़र्ज़ में मिलने वाली राहत या नए बनते फ्लाईओवर उसके लिए बड़ी और ज़रूरी ख़बरों में बदल जाते हैं। उसे अमेरिका की मंदी की फिक्र ज्यादा सताती है, विदर्भ की भुखमरी कम परेशान करती है। वह 20-25 करोड़ के एक छोटे से भारत का प्रतिनिधि हो जाता है जिसके लिए 80 करोड़ का एक विशाल भारत बस एक उपनिवेश भर है। कहते हैं, यूरोप की समृद्धि के पीछे 200 साल तक एशिया और अफ्रीका में चली औपनिवेशिक लूट का भी हाथ रहा है। हम यूरोप की टक्कर का एक भारत बनाना चाहते हैं और इसलिए भारत के ही एक हिस्से को उपनिवेश की तरह देख रहे हैं।
हिंदी और भाषाई मीडिया के लिए यह विडंबना दोहरी है। जो शासक और नीति-नियंता भारत है, वह अंग्रेज़ी बोलता है। इस अंग्रेज़ी बोलने वाले समाज के लिए साधनों की कमी नहीं है। वह इस देश की राजनीति चलाता है, वह इस देश में संस्कृति और साहित्य के मूल्य तय करता है, वह इस देश का मीडिया चलाता है। वह हिंदी या दूसरी भारतीय भाषाओं को इसलिए जगह देता है कि उसे बाकी भारत से भी संवाद करना प़डता है। लेकिन वह इन भाषाओं को हिकारत से भी देखता है, इन्हें बोलने वालों का संस्कार करना चाहता है, उन्हें अपनी तरह से बदलना चाहता है। साधनों से विपन्न गैरअंग्रेज़ीभाषी समाज भी इस अंग्रेजी का बड़ी तेज़ी से अनुकरण करता है। अचानक हम पाते हैं कि वह अपनी मौलिकता, अपने मुहावरे खो रहा है, एक अनजान, अख़बारी, स्मृतिविहीन, संवेदनारहित भाषा बोल रहा है। इसकी भरपाई वह सनसनी से, बड़बोलेपन से, शोर-शराबे से और इन सबके बीच मुमकिन हो सकने वाली एक स्मार्ट सी भाषा से करना चाहता है। हिंदी मीडिया के इकहरेपन की एक बारीक वजह यह भी है कि इसे अंग्रेज़ी वाले अंग्रेजी की तरह से ही चला रहे हैं। उन्हें लगता है कि हिंदी ऑटो ड्राइवरों, रेहड़ी लगाने वालों, उनके दफ़्तर के बाहर खड़े नीली-पीली वर्दी वाले संतरियों, दिहाड़ी के मजदूरों और ऐसे ही उन बहुत सारे लोगों की भाषा है जो पढ़े-लिखे नहीं हैं, जो सूक्ष्म संवेदना से अनजान हैं। इनके बीच हिंदी चैनल अपराध और सनसनी, अंधविश्वास और चुटकुले बेच कर ही चल सकते हैं।
बदक़िस्मती से अपनी ज़मीन और जड़ों से उख़ड़ा, अपने अभावों का मारा जो गरीब हिंदुस्तान महानगरों की कच्ची-पक्की, वैध-अवैध झुग्गी-झोपड़ीनुमा बस्तियों में रहता है और स्मृतिवंचित है, वह इस प्रभु वर्ग की धारणा की पुष्टि का आधार भी बन जाता है। इसके अलावा इस नए ज़माने के साथ कदम को मिलाने को बेताब और अपने घर-परिवार से बाहर निकल कर सिर्फ पैसा कमाने वाली नौकरी को ही सबकुछ मान बैठने वाला, और बड़ी तेज़ी से अपनी भाषा छोड़कर अंग्रेजी के ग्लोबल संसार से जुड़ने को उत्सुक जो एक और तबका है, वह भी मीडिया के इस मिथक को मज़बूत करता है कि हिंदी के लोग पढते-लिखते नहीं, गंभीर चीज़ों में रुचि नहीं लेते और उन्हें बहुत सतही क़िस्म की सूचनाएं चाहिए। लेकिन दरअसल यह वह खुराक नहीं है जो हिंदीवाला मांग रहा है, यह वह ख़ुराक है जिसका उसे आदी बनाया जा रहा है।
इस नितांत जटिल परिदृश्य में क्या कहीं कोई उम्मीद की किरण है? क्या इन हालात में हम ऐसा ही मीडिया भुगतने को अभिशप्त हैं? इस सवाल के जवाब कई हैं। मेरे भीतर जो बात भरोसा पैदा करती है, वह यह है कि हिंदी धीरे-धीरे सवर्णों की भाषा नहीं रह जा रही है। वे अंग्रेजी की तरफ मुड़ते जा रहे हैं। लेकिन इस देश के करोड़ों, पिछड़ों, दलितों और आदिवासियों की भाषा अब भी हिंदी है जिनके घर बिल्कुल पहली पीढ़ी में स्लेट, कलम, कागज या कंप्यूटर का प्रवेश हो रहा है। ये वे लोग हैं जिनकी आवाज़ धीरे-धीरे मुख्यधारा के मीडिया में आ रही है। इसके अलावा नए माध्यमों की जो दुनिया है, वहां भी इनकी पहुंच बनी है, इनका दखल बढ़ा है।
सवाल है, क्या ये लोग कभी इस हैसियत या हालत में होंगे कि मीडिया के मौजूदा परिदृश्य को बदल सकें? कहीं ऐसा तो नहीं कि यहां तक पहुंचते-पहुंचते ये खुद बदल जाएंगे, जैसे अपने समाज में हम बहुत सारे लोगों को बदलता देख रहे हैं? इसका भी कोई इकहरा जवाब नहीं हो सकता। यहां आकर हमारा वह संसदीय लोकतंत्र हमारे भीतर कुछ उम्मीद पैदा करता है जिसे हम खूब गालियां देते हैं। यह सच है कि सत्ता और बाज़ार के मौजूदा गठजोड़ के बावजूद अबाध मुनाफाखोरी का जाल अगर कहीं टूटता है, कारपोरेट मंसूबे अगर कहीं नाकाम होते हैं तो इसके पीछे चुनावी राजनीति का ही बल है। यह राजनीति न होती तो दलितों, आदिवासियों की दुनिया की दुनिया कुछ ज़्यादा बेनूर, बदरंग और विस्थापित होती। इस राजनीति ने उनको जो कुछ ताकत और पहचान दी है, उसी से उम्मीद बंधती है कि वे कभी मीडिया की मुख्यधारा का हिस्सा होंगे और इसे अपने ढंग से बदलेंगे।
(दृश्यान्तर पत्रिका से साभार)