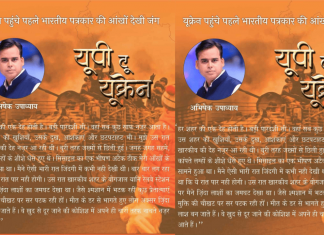लेकिन इसी दौरान( 12-14 दिसंबर) वीरेन्द्र यादव पवित्र पूंजी से संचालित जिस मंच पर पधारे, उसकी चर्चा अपने पाठकों से करना बिल्कुल भी जरूरी नहीं समझा. यहां तक कि अभी भी फेसबुक वॉल पर रायपुर महोत्सव को लेकर छोटी से छोटी टिप्पणी पर भी प्रतिक्रिया देने का काम जारी है लेकिन वहां भी संवादी में शिरकत को लेकर मौन हैं. क्या ये अकारण है ?
वीरेन्द्र यादव ने इस दौरान युवा और साहित्य को लेकर इस पवित्र मंच से क्या कहा, यदि कहीं इसकी चर्चा नहीं की, ऐसे में उनकी दिलचस्पी वहां लोगों ने क्या बोला, जाने-सुने बिना फरमान जारी करना रहा तो इसमे भला क्या आश्चर्य ? लेकिन किसी कार्यक्रम में शामिल होने भर से अगर किसी लेखक की प्रतिबद्धता निर्धारित होती है, तब तो ये बेहद जरूरी है कि लेखक के वक्तव्य पर बात करने के बजाय पूरी ताकत उस मंच की डीएनए टेस्ट में लगा देनी चाहिए चाहे.
वीरेन्द्र यादव को जिस रायपुर साहित्य महोत्सव से और संवादी दोनों से निमंत्रण मिला और इन्होंने फासीवादी सरकार के आयोजन के बजाय फासीवादी मीडिया को चुनना ज्यादा बेहतर समझा जबकि हमने रायपुर जाना तय किया. इसके पीछे वीरेन्द्र यादव जैसा कोई वैचारिक आग्रह नहीं था. बात फकत बस इतनी थी कि रायपुर के मुकाबले सात-आठ दिन की नोटिस पर लखनउ जाकर बोलने की योग्यता हम नहीं रखते. लेकिन क्या निजी सुविधा में लिए गए हमारे इस व्यक्तिगत फैसले को उतनी ही स्पष्टता से कॉर्पोरेट फासीवादी मीडिया का विरोध कहा जाएगा, जितनी सफाई के साथ वीरेन्द्र यादव जैसे लेखक के पहले ही चरण में मना कर देने का विरोध दर्ज किया गया ?
फासीवादी सरकार की जगह कॉर्पोरेट फासीवादी मीडिया को चुनना और ये जानते हुए कि फासीवादी सरकार का आयोजन है तो भी हां कहकर तब मना करना, इन दोनों स्थितियों में अपने को प्रतिबद्ध करार देने का जो सुख है क्या साहित्य की जमीन इसी से बची रह जाएगी ? ये बहस इस दिशा में भी बढ़ेगी जहां “आत्मावलोकन और आत्मालोचना की ईमानदार कोशिश “ के तहत फैसले लिए जाने के बावजूद फिसलन बरकरार रह जाते हैं?
ये सच भला किससे छुपा है कि जिस कॉर्पोरेट घराने ने संवादी कार्यक्रम शुरु किया है, उसने छत्तीसगढ़ तो छोड़िए, देशभर में फासावादी ताकतों, हिन्दूवादी रूझान की एकतरफा रिपोर्टिंग और यहां तक की पेड न्यूज की अपसंस्कृति विकसित की है और जिसका अर्थशास्त्र ही इस पर टिका है. 2009 के लोकसभा चुनाव में पेड न्यूज मामले में जिन दो अखबारों का नाम आया, उसमे एक नाम इसका( दैनिक जागरण) का भी है, जिस पर पीसीआई की रिपोर्ट से अपना नाम हटवाने तक का मामला सामने आया.
दूसरा, फासीवादी सरकार से इस मीडिया घराने का क्या संबंध है और इनके पूर्वज बाकायदा इसी बीजेपी के सांसद रहे हैं, क्या ये सब अलग से बताने की जरूरत है ? बाबरी मस्जिद विध्वंस से लेकर अच्छे दिन का बाकायदा अभियान इसके अखबार ने किस तरह चलाया है, इस पर भी किसी को शक हो सकता है ? ज्यादा नहीं इसकी सप्ताहभर की खबर को उठाकर देख लें तो भी ये समझ बनाने में मुश्किल नहीं होगी कि ये दरअसल उसी फासीवादी सरकार का मुख्यपत्र है जिससे हमारा विरोध रहा है और जिसके कार्यक्रम में वीरेन्द्र यादव जैसे पवित्र पूंजी से संचालित मंच की तलाश में निकले लोगों ने शिरकत की. वीरेन्द्र जिस प्रभावी विरोध की आकांक्षा रायपुर गए लेखकों से रखते हैं, क्या यही सवाल इस मंच से किया कि जो पैसे लेकर खबरें छापने के लिए ब्लैक लिस्टेड हुआ हो, वो किस नैतिक अधिकार के तहत अभिव्यक्ति का उत्सव करा रहा है ? ऐसे में क्या इस मीडिया घराने के कार्यक्रम को अपनी कवरेज से केन्द्र में फासीवादी सरकार कायम होने का जश्न के रुप में परिभाषित किया जा सकता है ? काश, निष्कर्ष इतने सपाट पाते. लेकिन नहीं, स्थितियां इससे कहीं अधिक विद्रूप है.
आप गौर करें कि पिछले कुछ सालों से साहित्योत्सव का चलन जिस भव्यता के साथ बढ़ा है, वो कॉर्पोरेट, कॉर्पोरेट मीडिया और अब कॉर्पोरेट की ताकत पर गठित सरकार की दिलचस्पी की परणति है. भव्यता और सुविधा के स्तर पर जिसकी वाजिब शिकायत और विरोध अलग-अलग मंचों से जारी है. इन तीनों क्षेत्रों से साहित्योत्सव के लिए जबरदस्त ढंग से पूंजी की पंपिंग हो रही है और इन तीनों के आयोजन में कॉमन बात है कि सबकुछ पीआर एजेंसी, ब्रांड चेहरे को ठेके लेकर बुलाने और इवेंट मैनेजमेंट कंपनियों के दम पर हो रहा है. क्या ये सवाल नहीं है कि जो अखबार, जो एफएम, टीवी चैनल साहित्य के लिए अमूमन पांच लाइन तक की जगह नहीं देते वो अचानक परिशिष्ट और स्पेशल स्टोरी पर कैसे उतर आते हैं ? क्या ये सब मुफ्त में, जनहित के तहत होता है ?
असल चिंता इस बात की है कि साहित्य और अभिव्यक्ति के नाम पर इन तीनों मंचों से जो अचानक से लाखों- करोड़ों रूपये लुटाए जा रहे हैं, उसके पीछे नियत सिर्फ छवि सुधारने की नहीं है. इसके भीतर राजस्व का एक ऐसा मॉडल विकसित करना है जो देश में पानी, बिजली, गैस की तरह कारोबार कर सके, सरोकार के भीतर भारी मुनाफे में तब्दील हो सके. जो काम पहले लोकतंत्र का चौथा खंभा के नाम पर मीडिया ने किया, अब साहित्य को “लिटरेचर इन्डस्ट्री” में तब्दील करने की कोशिशें हैं. हम जिस अलग-अलग नामवाची को लेकर जाने-न जाने का फैसला कर रहे हैं, अपने चरित्र और असर पैदा करने में एक-दूसरे से भिन्न नहीं हैं.
हम सरकार के बुलावे पर मना करके लेकिन फासीवादी कॉर्पोरेट मीडिया में शिकरत करने और खुद को बचाने का भ्रम भर पाल रहे हैं ? ब्रांड लेखकों को बुलाने या बुलाकर ब्रांड बनाने का जो चलन शुरु हुआ है, इस कारोबार में मुक्तिबोध से लेकर हवीब तनवीर सब जंचाए जा रहे हैं और सारा विरोध इसमे शामिल होने-न होने तक सिमट जा रहा है, क्या ये पूरा मॉडल जल-जंगल-जमीन के लूटे जाने, और उसके वाजिब हकदार को बेदखल किए जाने से साम्य नहीं रखता ?
वीरेन्द्र यादव ने संवादी अपने कहे की जो कहीं चर्चा नहीं कि लेकिन गूगल से जो दो पंक्तियां मिलीं, बिल्कुल सही है कि इसके लिए सिर्फ मीडिया और बाजारवाद दोषी नहीं, हम लेखक भी दोषी हैं.
मेरे ख्याल से हम दोषी इस अर्थ में भी हैं कि साहित्योत्सव को लेकर सारी कवायद वैचारिकी की जमीन को अर्थशास्त्र के अखाड़े में तब्दील करने की चल रही है और हम पार्टनर की पालिटिक्स जानने की नाकाम कोशिश कर रहे हैं. क्या दर्जनों साहित्यिक पत्रिकाओं के संपादक इसे रोक पा रहे हैं ? आखिर जिन मंचों पर जाने से लेखक कटघरे में खड़े किए गए, उन्हीं मंचों से विज्ञापन लेकर संपादक अब तक कैसे पवित्र बने रह गए ? इसी संवादी में क्या अखिलेश ने तद्भव की आर्थिक पवित्रता का नुस्खा वितरित किया ? मामला साफ है क्योंकि कटघरे में लेखक को खड़े करना फिर भी आसान है. इससे साहित्य के अर्थशास्त्र के बाकी अखाड़े सुरक्षित रह जाते हैं. फिर भी हमारा रायपुर जाना सध गया कि हम बेहद करीब से जान सके कि सरकार की मशीनरी, कॉर्पोरेट, पीआर एजेंसी, कॉर्पोरेट मीडिया और साहित्यिक ठेकेदारी के बूते जो साहित्योत्सव कराए जाते हैं, उसकी शक्ल कैसी होती है ? रायपुर साहित्य महोत्सव हम जैसे के लिए केस स्टडी है जिससे देशभर में जनतंत्र को मैनेजमेंट और मीडिया को उसका चाकर बनाए जाने की जो खुली खुली वर्कशॉप चल रही है, उसका विश्लेषण कर सके.
(मूलतः जनसत्ता में प्रकाशित)